जीवन के सपनों और उजास भरी आँखों के कविः जितेन्द्र श्रीवास्तव
यह दुनिया सिर्फ कहने में नहीं
अपने वजूद में भी बहुत बड़ी है
और जीवन चाहे जितना छोटा हो अरबों लोगों का
वह कुछ हजार लोगों की मुट्ठी में समाने से इंकार कर
अपनी जिद में आगे बढ़ जाता है
यही वजूद और यही जिद हम जितेन्द्र श्रीवास्तव के पहले कविता
संग्रह ’इन दिनों हालचाल’
से लेकर सद्य प्रकाशित पाँचवा संग्रह ’कायांतरण’
तक फैले उनके काव्य-संसार में भी देख सकते हैं। उनकी कविता ’कुछ हजार लोगों’ के जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि ’अरबों लोगो’ के जीवन तक विस्तृत है। गूँगा-बहरा बोधू
हलवाहा, गाँव-गाँव जाकर सेकुवा-हींग बेचने वाला शौका,
सब्जी बेचने वाला रामवचन भगत, मानसरोवर
यात्रियों का सामान ढोने वाले पोटर्स, लकड़ी-घास काटती-ढोती
पहाड़ी स्त्री , ट्रेन के डिब्बांे में गाना गाने वाली,
दुकान का नौकर ,ठेला खींचने वाला जैसे रोज
कमाकर खाने वाले श्रम से जुड़े पात्र ,लुंगी,बेना,पीढ़ा,लालटेन,कुदाल,बसुला,खुरपी,मूँज की खटिया,ढेकुल ,हाथ,सेई,जाँत,ढेंका ,ओखल जैसी साधारण पर रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं ,बथुवा,भुट्टा,धतूरा,जौ,केराव,बाजरा,निमोने जैसे उपेक्षित अनाज और पांगू ,छारछुम,
कनालीछीना , डीडीहाट ,थल
,बलुवाकोट,धारचूला,बभनान,रुद्रपुर,मगहर ,ओरछा ,बहराइच, देवरिया जैसे
अनजाने-अनपहचाने स्थान जितेन्द्र श्रीवास्तव की प्रतिबद्धता का पता बता देते हैं
कि उनकी कविता किसकी कविता है और उनका कवि-पक्ष किसका
पक्ष है। ये पात्र,वस्तुएं और स्थान मिलकर एक ऐसा
काव्य-संसार रचते हैं जहाँ अनाम कुल में जन्मे साधारण-सरल-विरल जन व उनकी विवशताएं
और सुख-दुःख पूरी जगह पाते हैं। उनके जीवन के दुखते-कसकते अनुभव आते हैं। उनकी
आवाज एक बड़ा वृत्त बनाती है। जितेन्द्र की ही कविताओं से शब्द लेकर हम कह सकते हैं
कि जितेन्द्र कवि हैं-जीवन के सपनों और उजास भरी आँखों के, उन
होठों के जिनको काट गई है चेैती पुरवा ,उन कंधों के जो धूस
गए हैं बोझ उठाते ,जिनको नहीं मयस्सर नींद आँख भर और नहीं
मयस्सर अन्न आँत भर ,उन उदास खेतों के दुःख के जिनको सींच
रहे हैं आँखों के जल ,जो नहीं काटते गला किसी का ,जो बने ओट हैं किसी फटी जेब के।यह कवि उनके बारे में सोचने के लिए
अनुप्रेरित करता है-जिनका अपनी साँसों पर ही अधिकार नहीं। साथ ही उन स्थितियों के
बारे में-जो चैन से खाने-सोने नहीं देता/बहुत उदास कर देता है मन। इस जीवन को
व्यक्त करना उनकी पहली प्राथमिकता लगती है जिसके लिए वे कहीं-कहीं काव्यात्मकता से
समझौते करने और भावुकता का आरोप सहने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस कवि का संकल्प
है- टुकड़े-टुकड़े में मिले जीवन के तारों को जोड़ना,अंधेरे में
डूब रहे मन को ढांढस बँधाना और निर्निमेष ताकती आँखों को सपना देना है। उनकी
कविताएं जीवन की चहल-पहल से भरी हुई हैं जिनमें पूरी जीवन-यात्रा के पड़ाव देखे जा
सकते हैं। वे जीवन के कोनों-कोनों की यात्रा कराते हैं। उनकी कविता हमारे आसपास और
दूर तक फैले जीवन की कविता है। जितेन्द्र जीवन की छोटी सी छोटी घटना, स्मृति ,वस्तु या संदर्भ को भी कविता में बदलने में
कुशल हैं। उनकी कविताओं में जीवन के विविध प्रसंग विवरणों की तरह आते हैं पर कभी न
बोझिल होते हैं और न ही सपाट। सहज ही अपने साथ शामिल कर बहा ले जाते हैं। हमारे
अनुभवों में साझीदार बनती हैं केवल विशिष्टता ही नहीं बल्कि विविधता और विस्तार के
साथ भी। इनमें बड़बोलापन नहीं बातूनीपन है। सृजनात्मकता के लिए अवकाश है। जितेन्द्र
असुंदर में सुंदर देखने वाले कवि हैं। वह वहाँ सौंदर्य देख लेते हैं जहाँ कोई और
नहीं देख पाता। वह नए सौंदर्यबोध की सृष्टि करते हैं। दूसरे के भीतर छुपे
सौंदर्यबोध को पढ़ लेते हैं।
स्मृतियों में जाना नहीं है चुनना कोई सुरक्षित कोना
जितेन्द्र कहीं स्मृतियों से तो कहीं सीधे परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी बात कहते हैं। जैसा कि उनके दूसरे कविता संग्रह ’असंुदर सुंदर’ के ब्लर्व में लिखा गया है,’’ स्मृतियों में बार-बार लौटना जितेन्द्र की कविता की एक खास प्रविधि है।’’ स्मृतियाँ उनके यहाँ अनायास नहीं बल्कि सायास आती हैं। एक औजार के रूप में वे उनका इस्तेमाल करते हैं। उनकी-निगाहों की अलगनी पर/टँगा है स्मृतियों का वसन/जो आज तक नहीं सूख पाया/पिछले कई वर्षों में। इसी का परिणाम है कि पहाड़ से उतरने और जे.एन.यू. से निकलने के बाद भी वहाँ के जीवन को कुछ इस तरह से व्यक्त कर पा रहे हैं जैसे कल की ही बात हो। स्मृतियों को जिंदा वही रख सकता है जिसको उनसे रागात्मकता हो। इसीलिए पहाड़ से लौटने के वर्षों बाद भी उनकी आँखों में बचा है-रक्त से लाल एक फूल बुरूँस का। उनके लिए ’स्मृतियाँ’ सूने पड़े घरों की तरह हैं। स्मृतियों को लेकर उनकी राय बिल्कुल साफ है-कुछ लोगों को लगता है/जैसे स्मृतियाँ पीछे ले जाती हैं हमें/लेकिन ऐसा होता नहीं हैे/स्मृतियाँ अकसर तब आती हैं/जब सूख रहा होता है/अंतर का कोई कोना/सूखे के उस मौसम में/वे आती हैं बरखा की तरह/और चली जाती हैं/मन उपवन में सींचकर। उनसे मेरी भी सहमति बनती है। स्मृतियाँ उम्मीद का एक सूत होती हैं। उनका जीवन में बहुत महत्व है। ये आदमी को जीने की ताकत देती हैं। उदासी से बाहर निकालती हैं। अकेले में साथ निभाती हैं। ढाँढस बँधाती हैं। थकावट बाँटती हैं। जितेन्द्र ’लौटना किस वजन की क्रिया है’ कविता में कहते हैं-जो नहीं जानते स्मृति सत्य/वे नहीं जान सकते/स्मृतियों में जाना हमेशा सुख में जाना नहीं होता/स्मृतियों में जाना नहीं है चुनना कोई सुरक्षित कोना/वे नहीं जान सकते /लौटना किस वजन की क्रिया है/आदमी लौट पाए तो जरूर लौटना चाहिए उसे/अपने जीवन से छूट गए/अलग-अलग घाटों चैराहों पर ठहरना चाहिए।
कहीं कोई फर्क नहीं था रोटी में
जितेन्द्र उन युवा कवियों में से हैं जो अपनी बात को कहने के लिए जनपद की प्रकृति,जन-जीवन और उसके संघर्ष को आधार बनाते हैं और लोककथाओं ,लोकगीतों व लोकस्मृतियों का सुंदर और प्रभावशाली उपयोग करते हैं। भले ही उन्होंने शहरीय और महानगरीय जीवन को लेकर भी अनेक कविताएं लिखी हैं पर उनका मन जनपदों में ही अधिक रमता है। यही कारण है कि उनकी कविताएं पढ़ते हुए मुझे प्रसिद्ध उपन्यासकार न्गुगी वा थ्योंगो का यह कथन बार-बार याद आता रहा-’’सभी मानवीय समुदायों का आधार है-मिट्टी और जमीन। बिना मिट्टी के बिना जमीन केे ,बिना प्रकृति के मानव समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं है।’’ जितेंद्र श्रीवास्तव के यहाँ जनपदीय जीवन बहुत गहरे एवं व्यापक रूप में आता है।वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जीवन के स्रोत जनपदों में निहित हैं और रचना को चेतन ,सजीव और प्राणवान बनाना है जो उसे जनपदीय जीवन से जोड़ना जरूरी है। जनपदों से उनके सरोकार बहुत गहरे हैं। उनकी कविताओं में जनपदों की कठिन परिस्थितियों के साथ-साथ वहाँ के परिवेश का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह किसी खास जनपद तक सीमित नहीं है। उनकी कविताओं में जितना देवरिया आता है जो उनका गृह जनपद है उससे कम सीमांत जनपद पिथौरागढ़ नहीं। उनकी पहाड़ से जुड़ी कविताएं पढ़ते हुए किसी को थोड़ी देर के लिए भ्रम हो सकता है कि वह पहाड़ के कवि हैं। दरअसल पहाड़ उनकी कुछ समय के लिए कर्मस्थली रही। यह विशेषता उन्हें नागार्जुन से जोड़ती है। नागार्जुन जब जहाँ गए वहाँ की प्रकृति और जीवन पर उन्होंने कविता लिखी। उत्तराखंड के पहाड़ों के दृश्यों और जीवन पर नागार्जुन की अनेक कविताएं हैं। अपनी जन्मभूमि के प्रति स्नेह या लगाव तो बहुत सारे कवियों में देखा जाता है जो स्वाभाविक भी है पर दूसरे जनपद के प्रति भी उतना ही स्नेह-सम्मान रखना बड़ी बात है। एक कवि ही क्षेत्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर इस तरह देख सकता है। यह मुझे जितेन्द्र की कविताओं की सबसे बड़ी ताकत लगती है। उनके देखने में भावुकता नहीं है। उन्हें पहाड़ का केवल सौंदर्य ही नहीं दिखता बल्कि उसका कठिन जीवन और संघर्ष भी उनकी आँखों से ओझल नहीं होता है। वे पहाड़ों के सौंदर्य को भी जानते हैं और उसकी मुश्किलों को भी-कितने सुंदर हैं पहाड़ /दूर से मैंने सोचा/कितने खुशनसीब हैं यहाँ के लोग/प्रकृति की गोद में रहते हैं/ मैं भी आया बसने पहाड़/जीवन पहाड़ हो गया।.....मैं पहुँचा पहाड़/मैं रमा पहाड़ में/ मैंने जाना वहाँ/कहीं कोई फर्क नहीं था रोटी में/हवा में उतना ही दुलार था/नींद में उतना ही घनत्व। जितेंद्र ने पहाड़ों में मीलों दूर से पानी सारते हुए महिलाओं को भी देखा है। कैसी विडंबना है-ये पहाड़ हैं नदियों के पिता/इनकी बेटियाँ सींच रही हैं मैदान/मैंदानों के मैदान/पर इनके घर में ही नहीं पानी।
विकास की धारा से दूर और पिछड़े क्षेत्रों और समाजों को
लेकर तथाकथित मुख्य धारा के समाज में अनेक मिथक प्रचलित होते हैं। उस समाज के लोग
हमेशा इन्हें हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में इन क्षेत्रों के बारे
में अनेक उल्टी-सीधी धारणाएं बैठी होती हैं। पहाड़ भी इनसे अछूते नहीं है। एक कवि
हमेशा इस तरह की सुनी-सुनायी बातों के खिलाफ होता है और उसका खंडन करता है। अपनी ’पहाड़ को जानना’ कविता में वे पहाड़ के बारे में
प्रचलित इस एकांगी धारणा को खंडित करते हैं कि-सूर्य उदित/पहाड़ मुदित/सूर्य
अस्त/पहाड़ मस्त/हो सकता है कुछ लोगों के लिए/यह सच हो/ दूध के रंग जितना/पर इसे
पूरा-पूरा सच मान लेना पहाड़ का/बहुत कम जानना है/पहाड़ को। ऐसा वही कवि कह सकता है
जिसको जनपदीय जीवन और वहाँ के लोगों से प्रेम हो। पहाड़ के लोगों के बारे में यह
गलत प्रचार है कि वहाँ के लोग शाम होते ही शराब के नशे में डूब जाते हैं जबकि यह
स्थिति कमोबेश देश कि विभिन्न जनपदों में देखने को मिल जाती है। वास्तव में यह
मानना पहाड़ को बहुत कम जानना है। कवि के मन में पहाड़ के प्रति कितना सम्मान की
दृष्टि है इन पंक्तियों से पता चलता है-ये पहाड़ हैं प्रिये!/देश की देह पर ढाल से।
यहाँ पर ढाल उस परम्परागत अर्थ में नहीं कहा है जिसके तहत हिमालय को उसकी ऊँचाई के
चलते भारत का रक्षक कहा जाता है बल्कि यहाँ के उन फौजियों को याद करते हुए कहा गया
है जो सीमा में तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और जिनकी पत्नियाँ जंगल में
घास-लकड़ी काटते हुए उनके सकुशल घर आने के गीत गाती हैं। कवि को पता है ’बादल कितना बदल देते हैं पहाड़ को’। बादल का छाना जहाँ
उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है वहीं उनका फटना आपदा को आमंत्रित कर देता है।
जितेन्द्र इन दोनों स्थितियों के गवाह हैं। उन्होंने धारचूला में रहते हुए काली
नदी का गैल-गम्भीर रूप भी देखा है और रौद्र रूप भी। धारचूला की पहाड़ियों पर चढ़ आई
धूप भी और पंचाचूली की चोटियों में पिघल रही बर्फ भी। बलुवाकोट-मुनस्यारी में गिर
रहे सुंदर झरने भी। ’तिब्बत’ की ओर
जाते हुए बादल भी। इन कविताओं में दर्ज हैं-पहाड़ों के रंग और जंगल की हरियाली।
जितेन्द्र भले पहाड़ों में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे लेकिन
जितना भी रहे उनका प्रयास पहाड़ों को अधिकाधिक जानना-समझना रहा। उन्हें जहाँ भी
पहाड़ को जानने का अवसर मिला उसको हाथ से नहीं जाने दिया। अर्थशास्त्र और संविधान
पढ़ रही किसी पर्वत सुंदरी से मिलकर पत्थरों-पहाड़ों में बसे जीवन का इतिहास जानना
चाहते हैं। वे पूछते हैं-क्यों वीरान हो जाते हैं तुम्हारे गाँव/जवान होते लड़कों
से। यह पहाड़ की बहुत बड़ी बिडंबना रही है कि उसका पानी और जवानी वहाँ ठहर नहीं पाए।
बह कर मैदान में पहुँचना उसकी नियति बन गई है। राज्य बनने के बाद भी यह सिलसिला
जारी है। जितेन्द्र ने अपनी कविताओं में पहाड़ के इस दुःख को बहुत बारीकी से पकड़ा
है। साथ ही पकड़ा है उन सैकड़ों दीदियों-भुलियों की उम्मीदों को जिन्हें उम्मीद है
एक दिन जरूर लौटेगा उनका बचपन में ही घर से भाग गया भाई।
कवि ’दुःख का पहाड़’ कविता में
अर्थशास्त्र और संविधान पढ़ती हुई युवती से यह प्रश्न पूछते हुए कि-तुम जानती होगी
विकास के सिद्धांत/तुमने पढ़े होंगे बड़े-बड़े नियम-कानून/हो सकता है तुम/जोड़-घटा लो
बहुत कुछ/पर क्या लगा सकती हो हिसाब/बता सकती हो आँकड़ा/पहाड़ के दुःख का? इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की नई पीढ़ी को पहाड़ की बदहाली के कारणों
को समझने और उसके खिलाफ उठ खड़े होने का सुझाव देते हैं।
वे आम पहाड़ी के यथार्थ से परिचित हैं। मानसरोवर यात्रा में पोटर्स के रूप में गए पहाड़ पुत्रों के बहाने हर श्रम करने वाले की स्थिति को सामने रखते हैं-वे जितना उठा पाते हैं/अपनी पीठ का बोझ/उसी अनुपात में भरता है/घर के लोगों का पेट।......वे महीनों के बाद लौटते हैं/अपने घरों को/पेट-पीठ एक किए हुए......अपने घरवालों की अनुपस्थिति में /अक्सर सोचती हैं ये घरवालियाँ/जो इनके घर भी होते भरे-पूरे/तो कौन उठाता बोझ/तो कैसे पाते ये पुण्य कमाने वाले मोक्ष। जितेन्द्र संवेदना के धरातल पर बहुत गहरे उतरने वाले कवि हैं इसलिए उनके मन से पहाड़ नहीं उतरा शायद उतरेगा भी नहीं। वहाँ से उतर आने के वर्षों बाद भी उनके आँखों में बचा है-रक्त-सा लाल एक फूल बुरूँस का। इसका कारण वह खुद बताते हैं-समय के साथ छूट जाते हैं बहुत से लोग/समय के साथ भुला जाते हैं बहुत से लोग/पर कुछ-न-कुछ होता है ऐसा/जिस पर नहीं चढ़ती है समय की धूल।
पहाड़ को जानने-समझने की ईमानदार कोशिश के बावजूद कहीं-कहीं जितेन्द्र पहाड़ विषयक कविताओं में चूक भी कर गए हैं। जैसे-पहाड़ों मंे आ रही है ठंड/जैसे आती है बीमार की आँखों में चमक....जैसे युद्ध के बाद आते हैं फौजी घरों को.....जैसे आती है रौनक विरहणी के चेहरे पर। इन बिंबों से ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों में ठंड का आना किसी खुशी की तरह है जबकि वास्तविकता यह है कि पहाड़ों में ठंड का आना सबसे पीड़ादायी है यहाँ के लोगों के लिए। इसी तरह एक कविता में वह शौकों को अपने भेड़ों के साथ मार्च में पहाड़ों से नीचे उतरते दिखाते हैं जबकि चरवाहों का नीचे उतरने का समय सितम्बर से शुरू होता है मार्च में तो वे ऊपर चढ़ने लगते हैं। पर इन्हंे बहुत बड़ी चूक नहीं कहा जा सकता है।
अभी बाकी है बहुत से लोगों में प्रतिरोध जैसी आदत
उनकी कविताओं में अपने समय का तकलीफदेह सच और अपने आस-पास की सुंदर दुनिया के साथ-साथ असुंदर दुनिया का प्रतिरोध है। प्रतिरोध भले ऊपरी तौर पर न दिखाई दे लेकिन वह अंडर टोन उपस्थित है। किसी भी कविता में बदलाव की चाह अपने-आप में प्रतिरोध का प्रतिरूप ही होता है। उनकी कविताएं बदलने के लिए आगे आने का आह्वान करती हैं। कुछ इस अंदाज में-इन्हें पी जाओ बौद्ध भिक्षुओ/और कर सको तो करो कुछ ऐसा/जिससे मुस्करा उठे वादियाँ तिब्बत की। प्रतिरोध का यह स्वर उनकी बहुत सारी कविताओं में मिलता है। एक उदाहरण ’दुःख पहाड़ का’ में भी देखा जा सकता है। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं-जैसे उसे याद होगी/धारचूला के सिनेमा हाॅल में देखी हुई पहली/जिसमें जुल्म के खिलाफ लड़ता है हीरो। यहाँ जुल्म से लड़ते हीरो का जिक्र करना यूँ ही नहीं है। उसके गहरे आशय हैं। ’असंुदर-सुंदर’ कविता में गूँगा-बहरा बोधू हलवाहा-’प्रतिरोध में पी जाता था अपने आँसू’। प्रथम दृष्ट्या यह लग सकता है आँसू पी जाना कैसा प्रतिरोध है ? पर हम गहराई में जाकर देखे तो इस तरह के कमजोर लोग दूसरों की दया-करुणा या सहानुभूति पाने के लिए बात-बात में आँसू बहाया करते हैं और बोधू का ऐसा न करना अपने आप में प्रतिरोध ही तो है। प्रतिरोध का एक रूप यह भी है कि उनकी कविता का आदमी हिंदी का अखबार पढ़ रहा है-अपनी भाषा में/अपने देश और पूरी दुनिया को बूझता-समझता वह/जुड़ा है खुद से/उसे पता है अपनी जड़ों का/और यह भी/कि इस तरह वह अस्वीकार कर रहा है/आतताइयों का/कि वह अस्वीकार कर रहा है/अजगर की तरह दूसरी भाषाओं को लीलती/किसी भाषा का/कि वह विरोध कर रहा है/हत्याओं के साजिश का। कवि मानता है ,आज के दौर में अपने पक्ष में तनकर खड़ा होना ही एकमात्र विकल्प है अपने बचाव का। कवि को दुःखद आश्चर्य भी होता है कि ये कैसा समय है-जो लोग शिद्दत से याद करते हैं/मुक्ति के शिल्पकारों-दार्शनिकों को/उन्हें सनकी करार दिया जाता हैे। ऐसे लोगों को पिछड़े और अप्रासंगिक करार दिया जाता है। पर कवि ऐसे लोगों की ओर उम्मीद से देखता है। उसका दृढ़ विश्वास है कि-दुनिया को बदलने के लिए/भीड़ की नहीं/विचारों और हौसलों की जरूरत होती है। कवि आश्वस्त है यह देखकर कि..... अभी सूखी नहीं है उम्मीद की नदी/अभी बाकी है बहुत से लोगों में प्रतिरोध जैसी आदतें। यही आदत है जो दुनिया को खत्म होने से बचाएगी और एक आम आदमी के रहने लायक बनाएगी। उनकी स्त्री विषयक कविताओं में भी जगह-जगह प्रतिरोध व्यंजित होता है। बेटियों का खिलखिलाना ,अपनी तरह जीना, मुक्ति की कामना करना, चिड़ियों की तरह उड़ने की कामना करना,अपने साथ हो रहे पुरुषवादी व्यवहार के लिए विधाता को कोसना आदि प्रतिरोध का ही परिचायक है। अदम्य जिजीविषा से भरी ’दूब’ के बारे में यह कहना कि- जमने को अपना अधिकार मानकर/देती आ रही है वह चुनौती/अपने खिलाफ साजिश करने वालों को/सृष्टि के आरम्भिक दिनों से। कहीं न कहीं प्रतिरोध के मूल्य को मान्यता देना है।
जितेन्द्र श्रीवास्तव ’तुरंता हो चुकी
इस दुनिया में’ हर स्तर पर बदलाव चाहते हैं और इसके लिए आगे
आने की जरूरत को महसूस करते हैं। उनका विश्वास बनी-बनाई परिभाषाओं को बदलते हुए नए
अर्थों को खोजने में है। लेकिन उन्हें ऐेसा बदलाव स्वीकार नहीं है जो अपनी जड़ों से
ही काट दे। अपने समाज-प्रकृति और जन से दूर कर दे। अपने ही शहर में ढूँढनी पड़े
अपने शहर की पहचान। दिखने लगे परायापन। लगने लगे बात और भाव और। कवि के लिए यह
विषाद की घड़ी है। अमेरिका की तरह मुँह करके कमर-कमर तक झुकने से जुड़ा बदलाव कवि को
स्वीकार नहीं है। केवल लोग ही नहीं ’बदल रहे हैं अर्थ’ भी। यह एल.पी.जी. का प्रभाव है।
संस्कृति बदल रही है। मूल्य बदल रहे हैं। स्वार्थ,लोभ-लिप्सा
हावी होती जा रही है। मानवीयता खत्म हो रही है। आदमी-आदमी के बीच अपरिचय बढ़ रहा
है। कवि इस तरह के बदलाव के खिलाफ है।
पानी की किल्लत गाँव से लेकर महानगरों तक बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं है-मिलता नहीं पीने को भी पानी। पर दुःखद है लोगों को पानी मयस्सर नहीं है और- हमारे प्रतिनिधि व्यस्त हैं/शक्ति के विमर्श और सत्ता के समीकरण में। पानी की किल्लत के चलते -ऐन राजधानी की जिह्वा पर बैठा एक आदमी/चाट रहा है अपनी होंठ प्यास से/और उसकी नाक पर बैठा आदमी/अपनी नाक पी रहा है प्रदूषित जल। जलाभाव तो कवि की चिंता का कारण ही है पर उन्हें बाहर के पानी के सूखने की चिंता से अधिक भीतर के पानी के सूखने की है-चारों ओर पानी ही पानी था उन दिनों/यह और बात है कि आँखों में पानी अब कम दिखता था/और नई पीढ़ी डूबने लगी थी/रंगत और नमक के जादुई विज्ञापनी समुद्र में।
रिश्तों के बीच आ गया है पैसा
पिता होना सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता
एक ’पिता’ की तरह एक कवि भी जिंदगी को कभी बंजर नहीं देख सकता है। माँ की ममता का कविताओं में खूब उल्लेख होता है पर पिता को लेकर बहुत कम कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। जितेन्द्र की कविताओं में पिता बहुत बार आते हैं। उनकी दृष्टि में-पिता होना सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता/जिम्मेदारियों में स्वयं को मिटाना होता है।..... अपने सपनों में खुद अनुपस्थित हो जाना/छोड़ देना उसमें बच्चों को/निश्छल किलकारियाँ भरने के लिए। कवि इस बात को समझता है कि स्वंय को मिटाना आसान काम नहीं है। पिता अपनी बची हुई आशाओं को हमारे सपनों में घोलते हुए ’समय की कहानी’ सुनाते हुए कहते हैं-हमें भूलना नहीं चाहिए/कि हम गुलामी के खिलाफ उबले/उस खून की विरासत हैं/जिसमें ’हम गलत वक्त में पैदा हुए’/यह कहने से बेहतर होता है/ ’अपनी पैदाइश को सही साबित करना’। इस तरह से पिता हमें नीर-क्षीर विवेक और साहस प्रदान करते हैं। कवि पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है यह जानते हुए भी कि यह संभव नहीं है .....धन्यवाद पिता /कि आपने चलना सिखाया/ अक्षरों/शब्दों/और चेहरों को पढ़ना सिखाया....कि आपने मेढ़ पर बैठना ही नहीं/खेत पर उतरना भी सिखाया.....सिर्फ काम करना ही नहीं /काम करना भी सिखाया........कि आपने लेना ही नहीं/उऋण होना भी सिखाया।
बेटियाँ होती ही शहद हैं
जितेन्द्र श्रीवास्तव की कविताओं में बेटियाँ बहुत बार आती हैं जिससे प्रमाणित होता है कि बेटियाँ उनकी प्राणशक्तियाँ हैं। जब एक ओर लड़कियों को जन्म ही नहंी लेने दिया जा रहा हो कवि का बेटियों को-इतने सुंदर इतने मोहक/नहीं सृष्टि में दूसरे फूल’ कहना सचमुच गहरा संतोष प्रदान करता है। ’ओ मेरी बेटियो याद रखना’ कविता में उनका यह कहना-तुम लोगों के आने के बाद/शायद मनुष्य होने लगा हूँ/तुम लोगों की हँसी में हँसने लगा हूँ। बेटियों के प्रति उनके लाड़-प्यार को व्यक्त करता है। वे बेटियों की जिह्वा पर विराजती पवित्रता और होंठों की हँसी को हमारे समय में जीवन की आशा के रूप में देखते हैं। भ्रूण हत्या तथा बेटियों के प्रति क्रूर दुनिया के विरुद्ध यह उनका अपने तरह का प्रतिरोध है। वे बेटियों से उदासी के बीच भी खिलखिलाते रहने की अपील करते हैं ताकि बचा रहे जीवन और बचा रहे विश्वास। वे खुद से भी बढ़कर मानते हैं बेटियों को और उनसे याद रखने को कहते हैं कि- यदि जीवन में दुःख का आलाप दीर्घ होने लगे/तब भी परछाइयों के पीछे-पीछे मत भागना/डरना नहीं किसी आइने से ......न डरना न हारना/लड़ना समय से। ये अच्छी बात है कि पग-पग पर समझौतापरस्त दुनिया में वे किसी समझौते में जाने की बात नहीं कहते हैं। बेटियों के प्रति उनका स्नेह अद्भुत है। बेटियों को स्वप्न और अपनी बदली हुई तकदीर मानते हुए कहते हैं-कि धूप हो तुम लोग/हम दोनों के जीवन के बसंत की। उन्हें इस बात में खुशी होती है कि उनकी छोटी सी बेटी-अपनी नन्ही-सी अँजुरी में/भर रही है कुछ बूँदें/मिला रही है उसमें रंग। बेटियों के प्रति इतना उदात्त स्नेह बहुत कम पिताओं में देखने को मिलता है। भ्रूण हत्या के इस दौर में उनका यह स्वर आश्वस्तिकारक प्रतीत होता है-इस समय मन में उजास है/उसमें टपकता है शहद की तरह/बेटियों का स्वर/बेटियाँ होती ही शहद हैं/जो मिटा देती हैं/आत्मा की सारी कड़वाहट। बेटियाँ उनके संसार में हमेशा नरम धूप की तरह बनी रहती हैं। बेटियों के चेहरे में जितनी हँसी देखते हैं वे उतनी ही उजास आ जाती है उनके जीवन में और बेटियों की उदासी उनके लिए किसी अंधेरे से कम नहीं है। पहली बार जब पापा शब्द सुनते हैं अपने आप के लिए उनके मन की मुण्डेर पर चाँदनी उतर आती है़़़़़़। ’मैं इक चिड़ियाँ हूँ पापा!’ कविता में वह बेटियों की आकांक्षा को व्यक्त करते हैं-धरती चिड़िया के पास है/आसमान उसकी आस है/पंख उसके पास हंै/बिना रोक-टोक वह उड़ती है/थक जाए तो/जिस टहनी पर चाहती है/बैठती है/गीत अपने गाती है। वह बेटियों के लिए भी इसी तरह की बंधन मुक्त दुनिया चाहते हैं।
स्त्रियाँ कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों कोजितेन्द्र केवल अपनी बेटियों से ही स्नेह नहीं करते हैं बल्कि पूरी स्त्री जाति से स्नेह करते हैं। इसलिए उनकी आँखों से बहती जलधारा में नमक की मात्रा बता पाते हैं। इसे वे पीड़ित खदबदाती आत्मा का जल मानते हैं। एक ’नमक हराम’ पुरुष इसके अनुपात को नहीं जान सकता है। कवि स्त्री के दुःख की गहराई की तुलना समुद्र से करता है। उनके प्रति कवि के मन में गहरा सम्मान है। तभी तो वे यह कह पाते हैं -वे रचती हैं/वे रचती हैं तभी हम-आप होेते हैं/तभी दुनिया होती है/रचने का साहस पुरुष में नहीं होता/वे होती हैं तभी पुरुष/पुरुष होते हैं। ऐसा समर्पण हमें भक्त कवियों में आत्मा का परमात्मा के प्रति ही दृष्टिगोचर होता है। स्त्री उनके लिए केवल आकर्षण ही नहीं सम्मान की भी पात्र हैं। उनका विश्वास है कि ’स्त्रियाँ कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को’। उन्होंने स्त्री पात्रों पर अनेक कविताएं लिखी हैं जिनमें वे स्त्री के पक्ष में और पुरुष वर्चस्व के खिलाफ खड़े हैं। साथ ही जीवन-जगत की सुंदरता और उसकी रचनात्मकता में स्त्री की भूमिका को रेखांकित करते हैं। इसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं दिखता। वे स्त्री के योगदान को स्वाभाविक और आत्मीय रूप से स्वीकार करते हैंै। उनके यहाँ मध्य और निम्न वर्ग की स्त्रियों का जीवन प्रमाणिकता के साथ आता है। स्त्री के दुःख-दर्द को व्यक्त करने के लिए वे लोक कथाओं का सहारा भी लेते हैं। लोककथाओं के माध्यम से अपनी बात कहने में जितेन्द्र दक्ष हैं। ’सोनमछरी’ और ’सोनचिरई’ इसी तरह की कविताएं हैं। सोनचिरई की कथा तो सीधे मर्म को छूती है। इसमें एक ग्रामबाला का सौंदर्य भी है और संघर्ष भी। हमारे समाज में एक निःसंतान स्त्री को क्या-क्या झेलना पड़ता है इस कविता में उसकी करूण अभिव्यक्ति है-ननद कहने लगी बज्रवासिन/सास कहने लगी बाँझ/और जो दिन-रात समाया रहा उसमें साँसों की तरह/उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की/अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो/तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसे में माँ भी उसका साथ नहीं देती है-माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को/नैहर में नहीं रहना चाहिए/लोग-बाग क्या कहेंगे/वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो। इसके बाद एक बेटी के लिए भला फिर कहाँ कोई जगह रह जाती है। जो लोग कभी पलकों में लिए चलते थे उनके यहाँ भी जगह नहीं उसके लिए। कैसी क्रूर दुनिया है यह?यही कारण है जिसके चलते एक औरत हर अन्याय-उत्पीड़न के सामने नतमस्तक हो जाती है। यह अजीब नहीं है कि सब स्वीकार करते हैं स्त्री का दुःख तो बड़ा है पर कोई उस दुःख को दूर करने के लिए आगे नहींे आता है। ऐसा क्यों है ? ’आभा चतुर्वेदी’ होना चाहती है आभा शर्मा और बनना पड़ता है आभा द्विवेदी। अपने जीवन के बारे में भी वह निर्णय नहीं ले सकती है?यह कोई आज की बात नहीं है सदियों से यही चला आ रहा है .....स्त्रियां अनादिकाल से पी रही हैं अपना खारापन/बदल रही हैं /आंखों के नमक को चेहरे के नमक मेें। उसकी नियति में शामिल है ..गरीबी में जीना/किसी हसीन शाम के लिए तरसना उम्र भर। जितेन्द्र स्त्रियों की आँखों की नींद और देह की थकान को महसूस करने वाले कवि हैं। उनके लिए किसी समुद्र की तरह स्त्री महज सौंदर्य नहीं है बल्कि पुरुष के जीवन को सजाने-संवारने वाली है।
उनकी ’लड़कियाँ’ कविता नहीं होना चाहती हैं। सजावट का सामान नहीं बनना चाहती। ’वे नहीं चाहतीं कि उन्हें बोझ समझा जाए...अपने जीवन के तमाम फैसले/स्वयं
करना चाहती है लड़कियाँ। उनके भीतर मुक्ति की तड़पन है। उनकी स्त्रियाँ जीवन में
पल-पल की घुटन से मुक्त होकर इंसान की तरह पूरे सकून से अपनी शर्तों पर जीना और
कहावतों से बाहर आना चाहती हैं। ’उन्हें बहुत अच्छा लगता
है/सरयू में नहाना।’ जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों के लिए
वर्जित माना जाता है। ’वे चिंता नहीं करतीं उन बातों की/जो
लोग करते हैं उनके बारे में।’ लड़कियों की इस बदलती सोच को
कवि हमारे समय की बड़ी घटना के रूप में देखता है। इस बदलाव के लिए ’परवीन बाॅबी’ जैसी अभिनेत्रियों के योगदान को
उल्लेखनीय मानता है जिन्होंने ठेंगा दिखा दिया था वर्जनाओं को ,किसी की परवाह नहीं की और अस्वीकार कर दिया था नैतिकता के बाहरी कोतवालों
को। अपनी शर्तों पर जीवन जिया। अपनी तर्ज से जी रहीं लड़कियों को हमारे परम्परागत
समाज में परियों की तरह देखा जाता है। ’सपनों में परी की तरह’
कविता कस्बे की लड़कियों के भीतर पल रहे सपनों की सुंदर अभिव्यक्ति
है। ’वे उड़ती हैं गौरयों की तरह’ कविता
में लड़कियों को निर्जला से तिजहर तक पीड़िया में गौरैयों की तरह उड़ते देखकर कवि खुश
होता है और कल्पना करता है-जो वर्ष भर होती पीड़िया/तो कितना चहकतीं लड़कियाँ। पर यह
चहकना अस्थायी प्रकृति का है असली रूप से तब चहकेंगी जब अपने पैरों में खड़े होकर
अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में होंगी। ऐसे कितने कवि
होंगे एक स्त्री को खुश देखकर जिनके ’रक्त में खुशी’ फैल जाती है और जो नीम की पत्तियाँ चबाने पर भी कम नहीं होती है मन की
मिठास। इससे एक कवि की संवेदना-स्तर का पता चलता है। पता चलता है कवि अपने पात्रों
से कितना एकमेक है। कवि के सपनों में स्त्रियों के लिए
एक ऐसे शहर की कल्पना है जहाँ लड़कियाँ अपनी शर्तों पर जीती हैं। ’जिस शहर का सपना है उसकी आँखों में’ कविता में
जितेन्द्र शहर के बहाने एक ऐसे समाज की का सपना देखते हैं जिसमें-..... कोई किसी
का राजा नहीं/कोई किसी की प्रजा नहीं/कोई किसी के अधिकार में नहीं रहता/कोई किसी
पर अत्याचार नहीं करता। कवि मानता है कि एक आदमी की तरह जीने के लिए ऐसा समाज
जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि कवि की स्पष्ट मान्यता है ऐसा समाज कोई ईश्वर
नहीं बल्कि आदमी ही बसाएगा। कवि अपने भीतर एक स्त्री की आत्मा लाना चाहता हैं-वह
भी एक ऐसे समय में/जब बच्चियाँ मारी जा रही हैं कोख में ही। वह सुनना चाहता है
उनसे उनकी और उनके जैसों की।
कवि को स्त्री पर काम का बोझ परेशान करता है जिसने वक्त से
पहले उसे बूढ़ी बना दिया है-यह स्त्री जिसे देख रहे हैं आप/यह तीस की उम्र
में/सैंतालिस की चिंताओं का घर है। इसका कारण उसके ऊपर अतिशय काम का बोझ है-वे
मुँह अंधेरे निकलती है/घरों से कलेवा बाँधे/और लौटती हैं साँझ ढल जाने पर/राह
टोहती हुई।......उस समय सहज नहीं होता/उनके भीतर की हलचल को जानना/जब पति को
खिलाती हुई रोटियाँ/वे खाती हैं गालियाँ.........वे भाग्य की बात करती हुई/हँसती
हैं विधाता पर/कभी कोसती है विधाता को/कहती हैं जो विधाता स्त्री होता/तो सोचो सखि
,कैसा होता। स्त्रियों का विधाता को कोसना एक तरह का विद्रोह
है पुरुषवादी समाज के प्रति क्योंकि स्त्री पर पुरुष के वर्चस्व को ईश्वर के नाम
पर ही वैध ठहराया जाता है। जितेन्द्र श्रीवास्तव परिवर्तन के आकांक्षी हैं पर किसी
हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में नहीं। सतत् विकास के क्रम में परिवर्तन को देखते हैं-
चलो खुश तो है एक बेटी किसी की/और भी होंगी धीरे-धीरे।
हमारे समाज में पुरुष और स्त्री के लिए अलग-अलग मानदंड
उन्हें उचित प्रतीत नहीं होते हैं। इनको लेकर उनके भीतर सवाल उमड़ते-घुमड़ते रहते
हैं-कि आखिर/सिंदूर क्यों लगाती हैं स्त्रियाँ/विवाह के बाद/विवाह तो पुरुष का भी
होता है/पर वह रह जाता है/जैसे का तैसा/उसके लिए कोई प्रतीक निर्धारित नहीं हमारी
परंपरा में। वे जानते हैं सामाजिक नियम-कानूनों के माध्यम से स्त्री की कंडीशनिंग
करने की कोशिश की गई है जिसका परिणाम है कि स्वयं स्त्री उनसे बाहर नहीं निकल पाती
हैं। इसका कारण कवि को पता है-.....कि सिंदूर भय है स्त्री का!/सोचता हूँ/जो डर
अनादिकाल से/घुला हुआ है/रक्त-मज्जा-विवेक में/वह कैसे निकलेगा/मीठी-मीठी बातों/और
छोटे-छोटे स्वार्थों से। ऐसा सवाल उसी कवि के मन में उमड़-घुमड़ सकता है जिसको
सामंती जकड़नों का अहसास हो। और इन सामंती प्रतीकों के पीछे का सच पता हो तथा उस
वर्चस्व की मानसिकता को समाप्त करना चाहता हो। उनकी एक
कविता है ’पुकार’ जो एक ऐसी स्त्री की
दास्तान है जिसका पति दारू ढकोसते हुए चल बसा और वह उनतीस की उमर में तीन-तीन
बच्चों की उँगलियाँ थामे’ खड़ी है चैराहे पर। न ससुराल मंे
कोई देखनहार है और न मैके में कोई पूछनहार। यह एक कटु यथार्थ है.....वैसे इस देश
में अकेली स्त्री नहीं है सुभागी/जिसे उसकी राय के बिना/बाँध दिया गया अनजान खूँटे
से.......पिताओ ,उठो ,कि बेटियाँ पुकार
रही हैं/उन्हें मत छोड़ो विधना की मर्जी पर/देखो उनकी भी मर्जी/उनको मत परोसो जीवन
भर की लाचारी/उन्हें हँसने दो उनके हिस्से की हँसी/उड़ने दो उनके हिस्से की उड़ान।
पर मुझे लगता है यह सब कुछ नहीं है पिताओं के हाथ। पिता कब चाहते हैं अपनी बेटियों
को ऐेसे लड़कों से ब्याहना। यह तो उनकी मजबूरी है।
गूलर का फूल न हो जाए प्रेम
प्रेम, कविता का सबसे पुराना विषय है। इस विषय पर अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है बावजूद इसके बहुत कुछ बचा हुआ है। हर कवि अपनी कविता में प्रेम के एक नए आयाम को उद्घाटित करता है। एक नए अंदाज में इसे व्यक्त करता है। प्रेमासक्ति और प्रेम की यातना इसके दो छोर हैं। प्रेम करना आसान हैं इसे निभाना कठिन है। जितेन्द्र श्रीवास्तव के यहाँ स्त्री के लिए पर्याप्त जगह है इसलिए प्रेम के लिए भी। प्रेम कविताओं के संदर्भ में वे केदारनाथ अग्रवाल की परम्परा का अनुसरण करते हैं। उनकी कविताओं में हमें स्वकीया प्रेम ही अधिक दिखता है और इन्हीं कविताओं में प्रेम की तासीर सबसे गहरी भी है। वैसे भी प्रेम की असली पहचान दाम्पत्य जीवन में ही होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दाम्पत्य प्रेम को प्रेम का सबसे उत्कृष्ट रूप कहा है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन का निर्वाह यथार्थ के कठोर धरातल में होता है। जीवन के रोज-मर्रा के संघर्ष वहाँ होते हैं। जीवन की आपाधापी होती है। इस सबके बीच यदि प्रेम जिंदा है तो वही असली प्रेम है। जितेन्द्र की कविताओं में यह दिखाई देता है-मेरे कदम भागते हैं हर साँस के साथ/मैं पहुँचता हूँ घर जहाँ/मेरी प्रतीक्षा से लंबी एक प्रतीक्षा/राह अगोरती मिलती है मुझसे। प्रेम की खासियत यही है कि आप जितना प्रेम देते हैं उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। मन देह की नदी में नाव बनकर बहने लगता है। ऐसी नाव जिसे किनारे की कोई सुध नहीं रहती है। कवि को पत्नी की अनुपस्थिति में घर की चाय गरमपानी की तरह लगती है। चाय का स्वाद नहीं रहता है। ऐसा केवल प्रेम में ही होता हैै। पे्रम पात्र की अनुपस्थिति में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए प्रेम का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान हैे उसे इन पंक्तियों से समझा जा सकता है....तुमने बदल दी मेरे लिए/जीवन की परिभाषा/और परिभाषाओं में खोया हुआ मैं/पा गया जीवन को। खिलखिला उठा मन ...सँभल गए डगमागाते कदम...उड़ गए दुःख के बादल...भर उठा आशाओं से......अपने ऊपर विश्वास बढ़ गया.... वह दूर पहाड़ में हों या फिर किसी महानगर में उन्हें पत्नी का चेहरा हमेशा याद आता है। यह बड़ी बात है। जितेन्द्र के लिए प्रेम जीवन के देैनिक क्रियाकलापों से अलग की जाने वाली कोई क्रिया नहीं है बल्कि जीवन में रची-बसी-पगी है। जो जीवन की तमाम गतिविधियों के साथ अपना स्पेस बनाती है। जीवन को सुंदर और सहज बनाती है। उनका प्रेम देह में उतरने की अपेक्षा आत्मा में उतरने की लालसा अधिक रखता है। उनकी मान्यता है- तब हम सुन सकेंगे शिकायतें एक दूसरे की पूरी निष्ठा से/हँस भी सकेंगे अपनी मूर्खताओं पर/और आजमा सकेंगे अपना प्रेम दैहिक आवेग से परे। प्रेम में वे पहचानते हैं-एक दूसरे का शरीर/एक दूसरे का सपना। घुलते हैं एक दूसरे में। रचते हैं एक दूसरे में कुछ। प्रेम में ही एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आज के प्रेमी-प्रेमिकाओं को देख कर उन्हें लगता है कि-बहुत तेजी से रिश्तों पर चढ़ रहा है रंग/बहुत तेजी से उतर रहा है उसका पानी। उनको लगता है कि ’तुरत-फुरत वाले इस युग में’ प्रेम अवारा पूँजी के नए पैकेज की तरह हो गया है जिसमें सब कुछ है पर भरोसा नहीं हैं। यह प्रेम ’आँख का पानी पीता हुआ’ है। वे प्रेम को किसी वर्जित फल की तरह नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि यदि प्रेम एक वर्जित फल बन जाए तो यह एक त्रासदी से कम नहीं होगा। उनकी चिंता है कि इस तरह महज शब्दों का अध्यवसाय बनते-बनते एक दिन कहीं ’गूलर का फूल न हो जाए प्रेम’। प्रेम विद्रोह है क्योंकि प्रेम में हम समाज के बने-बनाए नियम-कानूनों से सबसे भयंकर रूप से टकराते हैं।
हमारे लोक की अनगिन देह हैं ये लोग
लोक को लेकर इधर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। उसे गाँव के पर्यायवाची के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि लोक श्रम से जुड़े लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। वे गाँव में भी बसते हंै और महानगर में भी। जितेन्द्र किसी भ्रम के शिकार नहीं हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है-’यदि कोई देखना चाहे/हमारे लोक का चेहरा/वह देख सकता है/श्रम की आँच में तपे इनके चेहरे/इनके चेहरों पर/अपनी साँवली आभा के साथ/दिपदिपाता है हमारा लोक/हमारे लोक की अनगिन देह हैं ये लोग/इन्होंने पुतलियों की तरह बचाया है अपनी आत्मा को/ये पहरूवे हैं विश्वास के/ये पहचान हैं अपनी मिट्टी की। यही लोग हैं जिनके भीतर आज भी सबसे ज्यादा मनुष्यता बची है। लेकिन अभिजात्य वर्ग उसे हमेशा हिकारत की नजर से देखता है और उसका अपने हितसाधन के लिए उपयोग करता है। अभिजात्य वर्ग का लोक के साथ कैसा व्यवहार है यह उनकी कविता ’लोकतंत्र में लोक कलाकार’ में व्यक्त हुआ है। वे लोक कलाकारों की स्थिति को रेखांकित करते हुए कहते हैं देश-विदेश से आए सैलानी उतारते हैं उनकी फोटो विभिन्न कोणों से और समाजशास्त्री उनकी कला और वाद्ययंत्रों के बारे में लिखते हैं शोध-ग्रंथ पर नहीं पूछते कभी-कोई -उनके बच्चों की शिक्षा,उनके घर और उनकी गरीबी के बारे में/लेकिन वे जानते हें/लोक कलाकारों की तस्वीरें और उनकी दरिद्रता/खूब यश दिलाएंगी उन्हें और उनकी पुस्तक को। वे कभी नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में यह कहे- कि जब तक लोक कलाकार नहीं बोलेंगे/अपनी आवाज में अपना सच/नहीं लड़ेंगे अपने हिस्से की लड़ाई/तब तक लोकतंत्र/उनके लिए महज एक शब्द होगा/वह हलका होगा उनके लिए/अन्न,पानी और हवा जैसे शब्दों से। कवि चाहता है-लोक कलाकारों की जगह/रेत के टीले पर नहीं/ देश की आत्मा में होनी चाहिए.......कि जब कोई जाए किसी लोक कलाकार के पास/तो झुके उसी विनम्रता से/जैसे लोग झुकते हैं इबादतगाहों में।
लोक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही कही जाएगी कि वे ’लुंगी’ जैसे सर्वहारा के पहनावे को अपनी कविता का
विषय बनाते है। यह यूँ ही नहीं है। इस तरह के विषयों पर कविता लिखना दरअसल लोक
जीवन को प्रतिष्ठा प्रदान करना है। लुंगी सर्वहारा का वस्त्र है जो बहुउपयोगी है।
जब जैसा चाहें उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लोक जीवन में ही कोई वस्तु इतना
सम्मान और महत्व पा सकती है जहाँ वस्तु के प्रयोग का आधार आवश्यकता होती है न कि
दिखावा। अभिजात्य तो हर काम के लिए एक नई वस्तु का इस्तेमाल करता है। ’यूज एंड थ्रो’ के युग में लुंगी उपभोक्तावादी
प्रवृत्ति के खिलाफ खड़ी दिखती है- उसे कोई शिकायत नहीं होती अपने इस्तेमाल
पर/लेकिन वह टूटने लगती है तब/जब उसे जोड़ा जाता है/पिछड़ेपन और धार्मिक पहनावे से।
लुंगी की यह इच्छा-किसी धर्म किसी राष्ट्र की कैद में नहीे/किसानो-मजूरों के जीवन
में हीं/सुख का झंडा बनकर लहराना चाहती है। प्रकारांतर से कवि की इच्छा है। वह
किसी धर्म या राष्ट्र की कैद में नहीं रहना चाहता। यह कविता हमारी संवेदना को
झकझोरती है। इसी तरह बेना ,कटोरी ,लालटेन
जैसी छोटी-छोटी चीजें उनकी कविताओं के विषय बनते हैं। वह इन चीजों को भूलना नहीं
चाहते हैं।उन्हें पता है छोटी-छोटी चीजों से ही बनती है बड़ी दुनिया। विज्ञान और
तकनीक के युग में भी वह पुरानी चीजों की उपेक्षा नहीं करते। उनके महत्व को स्वीकार
करते हुए उचित सम्मान देते हैं। दरअसल यह निखालिस वस्तुओं को सम्मान देना नहीं है
बल्कि उनके बहाने उस जीवन को सम्मान देना है जो इनसे जुड़ा है।
लोकतंत्र उड़ा चुल्लू-चुल्लू
एक लोकधर्मी कवि ही लोकतंत्र को इस तरह कटघरे में खड़ा कर सकता है-मन उचाट पड़े हैं लोगों के/बहुतों के खाली हैं रसोईघर/बहुतों के तन पर वसन नहीं/कोई ओढ़ना नहीं घर में।.....लोकतंत्र उड़ा चुल्लू-चुल्लू/चारों ओर उल्लू-उल्लू। इसी का परिणाम है कि सरकारों की प्राथमिकता में आम आदमी कहीं नहीं हैैै। सरकार में बैठे लोग छोटे-छोटे प्रलोभनों के शिकार हैं। कहने को सामंतवाद समाप्त हो गया है लेकिन ’अब भी असंख्य ’होरियों’ की गर्दनें दबी हुई हैं/’नए रायसाहबों’ की/टाँगों के बीच।’ इसलिए कवि को लगता है कि यह मगन होकर नाचने गाने का समय नहीं है। शोषण-उत्पीड़न के कारणों या स्रोतों को पहचानने का समय है। व्यवस्थागत दोषों को समझने की जरूरत है। व्यवस्थागत दोषों को ईश्वरीय मर्जी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि-अकसर जिन चीजों से झाड़ना होता है पल्ला/उसे मढ़ देते हैं ईश्वर के सिर/लोगों के लिए ईश्वर/एक स्थायी सुविधा है/और लोकतंत्र में सरकारों के लिए/अमोघ अस्त्र। किसी को बोलने के हक से/इसलिए जुदा न किया जाए/कि उसे बोलने की कला नहीं आती। कवि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। कुदाल-आखिर क्यों नहीं ली जाती/प्रयोग से पहले उसकी राय/प्रजातंत्र के मतदाता/ और किसान की कुदाल में/ होना ही चाहिए कोई मूलभूत अंतर/ खेत की मेड़ पर खड़ी कुदाल/ सोच रही है/ और लोग चिंतित हैं/ कि कुदाल सोच रही है।
देश में एक और लगातार भूख-गरीबी-बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है दूसरी ओर सरकार मे ंबैठे लोग घोटाले-दर-घोटाले करते जा रहे हैं। कवि को यह बात कचोटती है कि भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। योग्यता की कोई कीमत नहीं रह गयी है। कवि इस रहस्य के बारे में समझना चाहता है-कि ऐसा कैसे हो राह है/कि जब टूट रहे हैं मनुष्य खिलौनों की तरह/तब कुछ लोग बातें कर रहे हैं विकास की......और बताइए कहीं यह एक शब्द’विकास’/पर्दा तो नहीं विनाश पर? विकास के नाम पर देश के संसाधनों को आँख मूँद कर निजी हाथों को सौंपा जा रहा है। सरकार लोककल्याणकारी कामों से लगातार अपने हाथ खींचते जा रही है। जनता के सपनों को नोच-नोच कर खा रही है। ऐसे में जितेन्द्र जायज प्रश्न खड़ा करते हैं....आखिर क्या करती हैं सरकारें/आखिर क्यों हैं सरकारें/क्या काम यही बस उनका/कि करें षड्यंत्र/लूटें मौज। वे इसके लिए जनता की निष्क्रियता को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए धिक्कारते हुए पूछते हैं कि आखिर जनता इस स्थिति को कब तक स्वीकार करती रहेगी। ’सबसे बड़ा दुःख’ कविता में कवि शासन के लोकल्याणकारी स्वरूप की अच्छी पोल खोलता है। सूखे ने सब चैपट कर दिया है। खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। प्रगति के इस मुकाम में मनुष्य की इससे बड़ी दुर्गत क्या हो सकती है। ऐसे में जब लोगों को सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए था दरिद्रता को भगाने के लिए सूप पीटने में लगे हैं। कवि को यह नागवार गुजरता है। वह दुःखी है इस स्थिति से। लेकिन कवि को ’सबसे बड़ा दुःख’ है कि लोग जानते हैं/आदमी पीपल का पेड़ नहीं होता/और न ही दरिद्रता कोई सूखी पत्ती/फिर भी इतने भोले बने रहते हैं/कि सूप पीटकर भगाते हैं दलिद्दर/और दरिद्रता अट्टहास करती है अपनी जीत पर। इस सब के बावजूद कवि को विश्वास है-आह के आग बनने में/भले ही लग जाए एक उम्र पर बनेगी।
’एक भाई का पत्र’ कविता में देश
की हालात पर कवि की गहरी चिंता व्यक्त होती है। सरकारों की उदासीनता पर व्यंग्य है
कि उसका क्या वास्ता बच्चों के सपनों से। कवि को पता है जनता के सपने कहाँ कैद
हैं। कौन हैं जो उसके सपनों को कैदमुक्त करने के नाम पर दिल्ली पहुँचते हैं और
वहाँ जाकर सबकुछ भूल जाते हैं उनका ’कायांतरण’ हो जाता है-लोग वर्षों ताकते रहते हैं उनकी राह/ताकते-ताकते कुछ नए लोग
तैयार हो जाते हैं/इसी काम के लिए। पर जनता का इंतजार कभी समाप्त नहीं होता है।
कवि ’कायांतरण’ कविता में रेखांकित
करता है-कि दिल्ली में एक और दिल्ली है-लुटियन की दिल्ली/जहाँ पहुँचते ही आत्मा
अपना वस्त्र बदल लेती है। इस दिल्ली में सब कुछ है पर वह एक खास वर्ग के लिए है।
जितेन्द्र यह बात मानने से इंकार करते हैं-कि यहाँ डाल-डाल पर सोेने की चिड़िया
बसेरा करती है/या कभी करती थी। दरअसल यह किसान-मजदूरों के पूर्वजों की रुलाई को
छुपाने का षड्यंत्र है। भ्रम फैलाने की कोशिश है। उनका सवाल जायज है कि-यदि ऐसा
है/या था/तो गरीब और जलालत का लंबा इतिहास/कैसे पसरा रहा लोगों के सिरहाने।कवि
मानता है कि यह इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाना है इसलिए आज नया इतिहास
लिखे जाने की जरूरत है। ’हमारा देश’ कविता
में इतिहास लेखन की परंपरागत शैली पर प्रश्न खड़ा किया गया है। वह सिनेमा जैसे
लोकप्रिय माध्यमों को कठघरे में खड़ा करते हैं-यदि लिखी होतीं लोगों ने/सबसे
लोकप्रिय माध्यम के लिए/भ्रम तोड़ने वाली रचनाएँ/तो शायद/कुछ कम होतीं किसानों की समस्याएं/तो
शायद किसान भी होते एकजुट/और बहुत संभव है/उनकी लड़ाई का नतीजा होता उनके पक्ष में।
हर बार बीज के साथ बोते हैं उम्मीद भी
जितेन्द्र किसान चेतना के कवि हैं। उनकी खुशी उन किसानों की खुशी में है जिनकी जान धरती के टुकड़ों में रहती है। ’नवान्न’ की खुशबू और पकी बालियों की चमक जिन्हें अभिभूत कर देती है। उनकी कविताओं में फसल को देखकर कृषक मन की खुशी को अनुभव किया जा सकता है। किसान जीवन से बहुत नजदीक से जुड़ा कवि ही ’नवान्न’ को देखकर एक किसान को होने वाली खुशी को ही इन शब्दों में व्यक्त कर सकता है-खेतिहर लोग इसे देखकर/वैसे ही फूलते हैं/जैसे बेटा होने पर/जैसे दुल्हन आने पर। किसानों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी चीज कवि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए ’बँसुला’,’खुरपी’,’कुदाल’ जैसे साधारण लेकिन जरूरी औजारों पर भी हमें कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। वह जानते हैं इनके बिना काम नहीं चल सकता है एक किसान का। उसके लिए हैं ये-रतन-की तरह/साँसों की तरह। जैसे-खुरपी न हो जिसके घर/गाँवों में/काम पड़ने पर/पलिहर का बानर हो जाता है वह.....बँसुला ईश्वर है काठ का/हाथ है बढ़ई का। कवि की प्रार्थना किसी अलौकिक शक्ति से न होकर खेतों से,पानी से, हवा से, धूप से,खाद से है। साथ ही अन्न से-कि मिलता रहे उसका स्वाद/मेरी जीभ को/मेरी आत्मा को। यही तो हैं किसान के सच्चे देवता। यह उनकी किसान चेतना का परिचायक है। जितेन्द्र की कविताओं में आए-ये वही किसान हैं कछार के/जो कभी-कभी ही काट पाते हैं/आषाढ़ में बोई फसल/इनकी खरीफ की फसल/समा जाती है नदी के पेट में/फिर भी ये नहीं हारते मन/तन-मन-धन से/धरती की कोख भरने में जुटे/ये किसान/हर बार बीज के साथ बोते हैं उम्मीद भी। वे किसान की पीड़ा को जानते उन कारणों को जानते हैं-जो दगा दे दें फसलें/दगा दे दे मिल/तो किसी जर्जर पुल की तरह/भारी हो जाता है किसान का जीवन।
दुनिया सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बनी है
जितेन्द्र ’आँखोे के जल में चेहरे’ देख लेने वाले कवि हैं। ऐसा वही कवि कर सकता है जो परकाया प्रवेश करने की क्षमता रखता हो। इसी के चलते वे घर से दूर रह रहे प्रवासी मजदूरों की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति कर पाते हैं। उनकी कविताओं में पहाड़ी, बिहारी,नेपाली मजदूरों की व्यथा-कथा समान रूप से आती है। उनके यहाँ ’खेलावन अहीर’ जैसे पात्र हैं जो श्रम में गहरी आस्था रखते हैं और मानते हैं कि-घुन लग जाएंगे शरीर में/रात-दिन खटिया तोड़ने से/जर जाएगी जवानी।.......रामजी, बिन जोते-कोड़े/घर में अनाज नहीं भर देंगे। यही है असली ’लोक का चेहरा’-ये मजदूर हैं/जो रोजी-रोटी की खोज में/निकल जाते हैं सुदूर प्रांतों में/उन जगहों में करते हुए काम/ये सोचते हैं अपनेे ’देस’ के बारे में/जहाँ इनकी स्त्रियाँ घरों में जूझती हुई जिंदगी से/राह अगोरती हैं इनकी। आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी ने जहाँ एक ओर हमारे जीवन को आसान बनाया वहीं दूसरी ओर श्रम के प्रति सम्मान को कम किया है। ’बैल’ कविता में यही भाव व्यंजित हुआ है-वे बैल जो हल से/चीर सकते हैं धरती का कलेजा/ढो सकते हैं सामान बैल गाड़ी में नधकर/अब साबित हो गए हैं पिछड़े। यही स्थिति आज श्रमशील मनुष्य की भी हो चुकी है। रोज कमाने खाने वाले लोगों के जीवन में कुछ नया नहीं है। वही रोज की रोजी-रोटी का संघर्ष। जी-तोड़ कोशिशों के बाद भी/दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं होता। पर उसकी जीवटता है कि वह.....सपनों को बेलगाम होने नहीं देता। यही लोग हैं जिनको ’सूर्य की घड़ी का ठीक-ठीक हिसाब’ पता है। कितना सटीक है कवि का यह कहना- आखिर सूर्य की घड़ी का ठीक-ठीक हिसाब/वही तो बताएंगे/जो उसकी आँखों में आँखें डाल/उससे हाथ मिलाएँगे!
’रामबचन भगत’ जैसी
कविताओं में गाँवों से पलायन की मजबूरी भी परिलक्षित होती है। रामबचन जैसे प्रवासी
लौटना चाहते हैं अपने गाँव पर लौट नहीं पाते क्योंकि-अब न गाँव बचा न खेत/सब समा
गए नदी के पेट में। कौन छोड़ना चाहता है अपना गाँव-जवार पर रोजी-रोटी की जरूरत इस
बात के लिए विवश करती है। यह क्रम बहुत पुराना है जो अभी तक भी नहीं थमा। यह
ऐतिहासिक तथ्य है औपनिवेशिक शासन के आने के बाद से जैसे-जैसे गाँव की आत्मनिर्भरता
समाप्त होती गई वैसे-वैसे गाँव छूटते गए। आज ग्लोबलाइजेशन के चलते एक ओर भले ही ’वैश्विक गाँव’ की गेंद खूब उछाली जा रही है पर दूसरी
ओर गाँव उजड़ते जा रहे हैं। शिक्षित हों या अशिक्षित सभी पलायन को मजबूर हैं। यह
बात हमें स्वीकारनी होगी कि गाँव जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और आधारभूत
सुविधाओं से सम्पन्न नहीं हो जाते पलायन का रूकना संभव नहीं है। गाँव में दो तरह
के लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं पहले, जिनके खेत-खलिहान नहीं
रहे रोजी-रोटी की तलाश में वे गाँव छोड़कर शहरों की ओर आते रहे हैं दूसरे, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की चाह में गाँव से निकल रहे हैं। दोनों के
कारण बाहर ही हैं। ’लोक का चेहरा’ कविता
में कवि ’लोकगीतों के रचे जाने के सदियों बाद’ भी रोजगार की तलाश में अपने मुलुक को छोड़कर सदूर प्रांतों में जाने की
विडंबना को उभारते हैं। साथ ही बिना अधिक बोले स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीतियों पर
एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं।
गाँव का छूटना मात्र गाँव का छूटना नहीे होता है ,उसके साथ छूट जाती है वहाँ की बोली बानी,खान-पान,
वेश-भूषा और भी बहुत कुछ जो जीवन में विविध रंगों को बनाए रखता है।
इस कविता में यह विडंबना बखूबी दर्ज हुई है। उस विडंबना की ओर भी संकेत हुआ है जो
आज हर संवेदनशील व्यक्ति की चिंता का कारण है-बहुत मार-काट है/इन दिनों/जिसे देखो/वही
धकियाते जा रहा है दूसरे को। कवि इस बात से पूरी तरह सहमत है कि-दुनिया सिर्फ कुछ
लोगों के लिए नहीं बनी है/यहाँ सबको हक है/अपनी भाषा/अपनी बोली/और अपने श्रम की
आजादी के साथ। जीने का।
बाजार के इतने चेहरे दिखते हैं एक साथ
कवि जितेन्द्र आज के नवपूँजीवादी-उदारवादी-बाजारवादी समय को शापित समय मानते हैं। इस समय में-बाजार के इतने चेहरे दिखते हैं एक साथ/कि मिथकों में साँस ले रहे सारे मायावी चरित्र/मिलकर भी नहीं बना सकते उतने चेहरे/वह बेधड़क समा जाता है/हमारे अंतरंग क्षणों में/वह पलक झपकते जान लेता है/हमारी साँसों का रहस्य/उसके पास हिसाब है/हमारी पुतलियों के हिलने-डुलने का/वह हमारी जीभ और आत्मा को/ रखना चाहता है अपने कब्जे में। इसके विपरीत ’अब नहीं आते वे’ कविता में जितेन्द्र उन शौका व्यापारियों का जिक्र करते हैं जो पहले गाँव-गाँव ,घर-घर जाकर सेकुवा ,गंदरायण,हींग, डोलू आदि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पायी जाने वाली वनस्पतियों को बेचा करते थे। उनके बारे में कवि का कहना है-वे बेचने वाले गारंटी होते थे/अपने माल की/उन्हंे अपना सामान बेचने के लिए/नहीं करना था कोई विज्ञापन/उनकी कोई साँठ-गाँठ न थी/किसी देशी-विदेशी कंपनी से। ये पंक्तियाँ मात्र शौका व्यापारियों की तारीफ में नहीं कहे गए हंै बल्कि उससे अधिक आज की लूटेरी बाजारवादी व्यवस्था पर चोट हंै। वे बाजारवादी कुचक्रों के बरक्स शौका व्यापारियों की सादगी और ईमानदारी को खड़ा कर देते हैं। कवि इस बात को अच्छी तरह समझता है कि समाज में अपराध के बढ़ने के लिए बाजारवादी अर्थव्यवस्था द्वारा युवाओं के मन में पैदा की जा रही अंध लालसाएं जिम्मेदार हैं। आज का युवा सपना देख नहीं रहा है उसके आँखों में सपने बोए जा रहे हैं। सपने भी ऐसे जो बाजार के हित में हैं जो उसकी भोगवादी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। इसमें सत्ता और मीडिया दोनों का बराबर का हाथ है। यह हमारे समय का कड़वा यथार्थ है। मीडिया आँख बंद किए हुए है उस ओर से जो इस प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है। उनकी कविता ’लालसाओं की पालकी’ में यह बात पूरी काव्यात्मकता के साथ व्यक्त हुई है-वह चमक किसी अघाए हुए आदमी की नहीं/एक बेरोजगार युवक की आँखों में थी......एक दिन अखबारेां में छपी उसकी तस्वीर/टेलीविजन पर दिखाई गयीं उसकी कई तस्वीरें/उस पर ईनाम था और वह फरार था......यह विभ्रम का समय है/पूरी पीढ़ी शिकार है विभ्रम की/मनोवैज्ञानिकों ने कहा यह विस्फोट है /अतृप्त आकांक्षाओं का /दिलचस्प यह भी/कि इन कार्यक्रमों के प्रायोजक/लगातार संलग्न थे /लोगों की अतृप्त आकांक्षाओं को जगाने में/जो लोग बताना चाहते थे उस जैसे युवकों के संघर्ष /उनकी हार अपमान और पीड़ा के विषय में/उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था/मीडिया और सत्ताएं मगन थीं/अपना-अपना राग अलापते हुए/और इनमें से कोई तैयार नहीं था/उस ओर देखने के लिए भी/जिधर से आ रही थी पालकी लालसाओं की।
सच कहिए तो सही प्रतिनिधि वही हैं जे.एन.यू. के
’तेरह वर्ष बाद एक दिन जे.एन.यू. में फिर’ एक अनूठी कविता है। इसके बहाने कवि ने एक पूरे दौर को याद किया है। इसे एक कालखंड का संक्षिप्त इतिहास कहा जा सकता है। इसमें जे.एन.यू. का पूरा परिवेश चित्रित हुआ है-उन दिनों जे.एन.यू. में इमारतें कम थीं/प्रकृति ही प्रकृति थी चारों ओर/बारिश में उठती थी/मिट्टी से सोंधी गंध/नृत्य करते थे मोर उन्मुक्त। साथ ही जे.एन.यू. में पिछले तेरह सालों में आए परिवर्तन इस कविता में दर्ज हुए हैं। कवि को-तब जे.एन.यू. में होना/सपनों के नगर में होना’ लगता था।.....जे.एन.यू. तमाम विश्वविद्यालयों की तरह/अपने में खोया ,संतुष्ट और आत्मरति से भरा हुआ न था।.....जे.एन.यू. नाम था एक आँच का/जो शीतलता देती थी स्वप्नधर्मियों की आत्मा को।.....विद्यार्थियों के लिए जे.एन.यू. पर्याय था/जीवन का संघर्ष का सपनों का। ....वह शरणगाह भी न था वामपंथियों के लिए/वहाँ कद्र थी अन्य विचारों की भी/कि विचार अग्रगामी बनाने वाले/ सपने पैदा करने वाले/और उनको परिणति तक पहुँचाने वाले हों।....सभी इस रंग में रंगे थे।....नहीं थे पहरे लड़के-लड़कियों की आवाजाही पर/लड़कियाँ आजाद परिंदों की तरह रहती थीं......जहाँ सबसे बड़ा मूल्य है आजादी। इस तरह जे.एन.यू.का पूरा चरित्र सामने आ जाता है। कवि इस बात को स्वीकार करता है कि हमने दूसरे को स्पेस और महत्व देने की कला वहीं से ही सीखी। यहाँ कवि अपने पुराने दिनों को ही याद नहीं करता है बल्कि जे.एन.यू. के कद में आई गिरावट और बदलावों को भी दर्ज करता है। ये बदलाव अचानक या केवल एक विश्वविद्यालय में आए बदलाव नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदार हैं-सोवियत संघ का विघटन,मनमोहन सिंह का वित मंत्री बनना, भारत की अर्थनीति का बदलना,उदारीकरण की हवा चलना, भूमंडलीकरण का दिया जलना ,भारत का मुक्त बाजार की खाई की ओर लुढ़कना ,उसकी विश्व बैंक के गलियारे की ओर चहलकदमी बढ़ना,अयोध्या कांड का अंधेरा ,मंडल कमीशन की गूँज आदि। इस सब का प्रभाव वहाँ के अध्यापकों और विद्यार्थियों में पड़ने लगा। जे.एन.यू. एक तरह से भारतीय प्रगतिशील राजनीति का चेहरा है जो आज धूमिल होता जा रहा है। उसमें एक धुंध छाती जा रही है। कवि की यह बात सही है- किसी भी कालखंड में/सब नहीं रंग जाते एक ही रंग में/जब चारों तरफ होता है श्याम रंग/तब भी कहीं-कहीं चमकता है सफेद बिजली की तरह। वास्तव में-यह हमारे समय की विडंबना है/कि हमारे बीच तेजी से कम हो रहे हैं/चंद्रशेखर जैसे ओजस्वी,तेजस्वी और निश्कवच लोग।’अजिताभ बाबू’ कविता में इसी बात को आगे हैं-कि जे.एन.यू. के लगभग चार दशक के इतिहास में/एक अकेले चंद्रशेखर हैं/जिन्होंने सचमुच लाँघा था परिसर।.......मित्रवर ,जीवन के जादू से बड़ा नहीं होता कोई जादू/लोग इसी में जनमते हैं और इसी में खप जाते हैं/जो अलग जाते हैं इस राह से/चुनते हैं प्रतिकार का जादू/सच कहिए तो सही प्रतिनिधि वही हैं जे.एन.यू. के। इन पंक्तियों में हमें कवि की राजनीति का भी पता चलता है। कवि के अनुसार प्रतिकार एक बड़ा राजनीतिक मूल्य है। जितेन्द्र इस बात को मानते हैं कि बहुत कुछ बदल जाने के बावजूद-बहुत कुछ बाकी है/और जो बाकी है उसको बचाने की जिद/होनी चाहिए सब में। इस कविता में आए ब्यौरे खटकते नहीं हैं बल्कि लगता है कुछ और होते तो कितना अच्छा होता।’कलकत्ते में सूरज’ उनकी राजनीतिक कविता है यह कोई प्रकृति का दृश्य नहीं - यह लो/यहाँ मिला /कलकत्ते में/ सूरज/सीना ताने/हम तो/कब से /चाह रहे हैं/इसे देखना/दिल्ली के सिरहाने।
अपने ही मन को हाथ देते
कवि के मन में अपनी बोली के प्रति गहरा लगाव है। महानगर में रहते हुए भी उनके मन का रसायन नहीं बदला है। कवि एक खालीपन महसूस करता है कि ’बहुत दिन हुए’ किसी के मुँह से नहीं सुने लोक बोली के कुछ खास शब्द। उन्हें नहीं लगते कोई शब्द गँवारू। वह अपनी लोकबोली के शब्द का उच्चारण कर ’अपने ही मन को हाथ देते’ हैं। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाषा के संस्कार मनुष्य के लिए उतने ही जरूरी होते हैं जितनी जरूरी होती हैं जड़ें किसी वृक्ष के लिए। इसीलिए जितेन्द्र अपनी कविता में बार-बार लोक बोली के शब्दों का सहज-स्वाभाविक रूप में प्रयोग करते हैं। अपनी काव्यभाषा को दुरुह नहीं होने देते हैं। उनकी भाषा कहीं भी संप्रेषणीयता में बाधक नहीं बनती है। भाषा-शिल्प को लेकर ’कायांतरण’ कविता संग्रह के ब्लर्व में लिखी इस बात से मेरी पूरी सहमति है कि जितेन्द्र अपनी पीढ़ी के शायद उन थोड़े रचनाकारों में हैं जो सिर्फ शाब्दिक भंगिमाओं के जरिए रूपवादी काव्यार्थ रचने में विश्वास नहीं करते।
जी सकते हैं कुछ पल प्रकृति से आइस-पाइस खेलते हुए
प्रकृति की विविध छवियाँ भी हमें जितेन्द्र के यहाँ दिखाई देती हैं जिनमें प्रकृति का उल्लास निहित है। वे अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए प्रकृति का सहारा लेते हैं। प्रकृति जीवन से उनकी निकटता यथार्थ को उभारने में तो सहायक बनी ही है साथ ही नए सौंदर्य की सृष्टि की है। उनकी कविताओं में हर मौसम के रंग बिखरे हुए हैं। कहीं धूप है तो कहीं शीत। कहीं-धूप की कई लकीरें/छू रही हैं होठ खिड़कियों के। कहीं.....हरीतिमा अठखेलियाँ करती है धूप से/धूप पहाड़ियों से। उनकी कविताओं में दिख जाते हैं- केले के गाछ की लंबी क्यारियाँ, वृक्षों से ढके टीले ,पंचाचूली में पिघलती हुई बर्फ, बलुवाकोट-मुनस्यारी में गिर रहे सुंदर झरने, रात की एकाकी में उतर रहा चाँद, धवल रूई के फाहे से उड़ते हुए बादल, चीड़-देवदारू के वृक्ष,बरसात में चढ़ आई काली गंगा,गोर्रा नदी ,पहाड़ की बरसाती शाम, सरयू नहाने गया अलसाया सूर्य , कलकल करती बहती जामिनी नदी, चीं-चीं करती हुइ गौरया .....जो सुंदरता का कोई और ही रूपक बनाते हैं। मन में घोलते हैं कुछ। कवि को भाता है-गर्मियों की शाम में/ स्टेशन की किसी खाली कुर्सी पर बैठकर/निहारना चिड़ियों को। उनकी कविताओं में कभी कातिक ,कभी सावन ,कभी बैशाख की झलकियाँ झलकती हैं।......चाँदनी रात में चमकती हैं अंकवार भरती पेड़ों की टहनियाँ.....सरोवर दिखता है बत्तखों से भरा हुआ......चाँद दिखता है तारों से अठखेलियाँ करता हुआ.....घोंसले की ओर लौटती हुई चिड़ियों की आँख में चमकती है साँझ...... चारों ओर पकी बालियाँ/सोने जैसी चमकती हैं। दिन भर का थका-हारा सूर्य घरौंदे की खोज में भटकते-भटकते चला जाता है किसी गुफा में ढलान से दूर बहुत दूर........जंगल में आधी रात को/फूटता है एक सोता। इस तरह उनकी कविता में प्रकृति की इंद्रधनुषी छटा के दर्शन होते हैं जो आज की कविताओं में बहुत कम होती जा रही है।
जितेन्द्र केवल समाजिक यथार्थ,विसंगति-विडंबना
और प्रकृति के ही कवि नहीं हैं वे जीवन-दर्शन के कवि भी हैं। मानव मन के विविध
संवेगों की उन्हें व्यापक एवं गहरी समझ है। वे मन के उल्लास को जितनी गहराई से
महसूस करते हैं उतनी ही सूक्ष्मता से दुःख का चेहरा पढ़ना जानते हैं। वे अच्छी तरह
जानते हैं- दुःख का वही चेहरा नहीं होता/जो दिख जाता है पहली नजर में.....जो नहीं
पढ़ पाते चेहरे के पार की भाषा/वे कभी नहीं जान पाते/दूसरे के भीतर का दुःख। उनका
जीवन-दर्शन है-दुःख आए/कोई बात नहीं/पर ऐसे आए/कि निरर्थक न लगने लगे जीवन/थका-थका
न लगे पुरुषार्थ/मरने न लगे संवेदनाएं/उसी में घुल-घुलकर.। उनकी कामना है.....कि
बचा रहे आँखों का पानी/बची रहे जीवन की रवानी। जितेन्द्र
दुःख से घबराते नहीं है। उसे हावी नहीं देते हैं,क्योंकि वह
जानते हंै-ये दिन बीत जाएँगे/धीरज धरो!/कुछ भी ठहरा नहीं रहता/न समय/न सुख/दुःख भी
नहीं। दुःख के प्रति यह दृष्टिकोण अवसाद मुक्त जीवन जीने के लिए जरूरी है। कवि
जितेन्द्र श्रीवास्तव की चाह है कि......कितना अच्छा होता/सब छोड़ जाते विरासत
में/चुटकी भर हँसी/मुट्ठी भर कोमलता/अंकवारी भर प्यार। एक कवि भला इससे ज्यादा
क्या चाह सकता है। यही तो है कवि होना। इस रूप में वे एक सच्चे कवि हैं।
..
महेश चन्द्र पुनेठा युवा कवि, समीक्षक
एक कविता संकलन "भय अतल में". सूत्र सम्मान से सम्मानित
संपर्क : punetha.mahesh@gmail.com
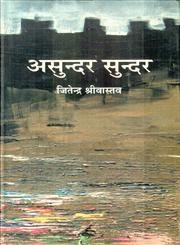








टिप्पणियाँ
अरुण होता
जैसे कि जितेन्द्र के कवि मन का रेशा रेशा खोलकर सामने रख दिया....सचमुच ....